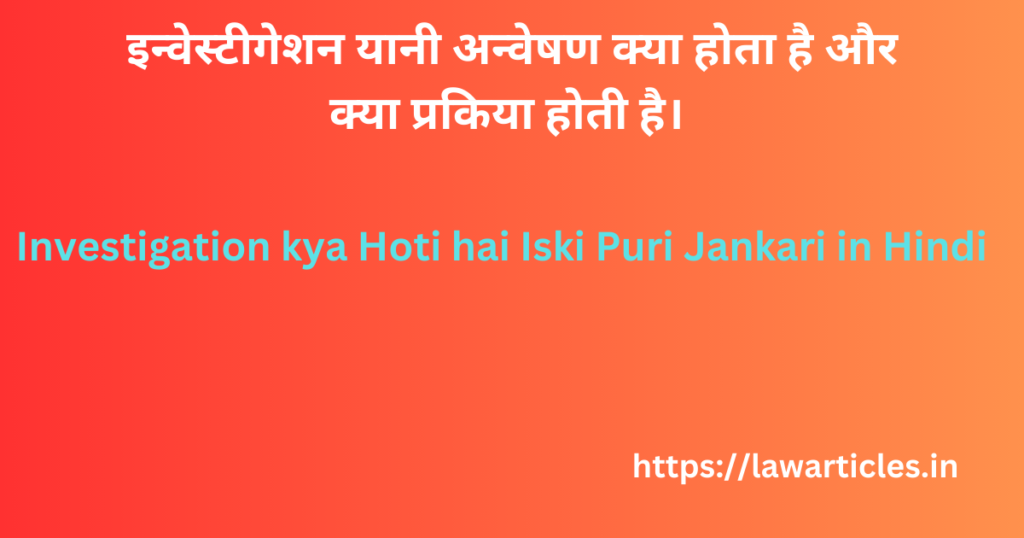
प्रणाम साथियो आज के लेख में हम सभी जानेगे कि इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण क्या होता है और क्या प्रकिया होती है। इसके बारे में इस लेख के माध्यम से आप को सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहा हुँ जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में उल्लिखित प्रकिया के तहत पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को क्या पावर है और यह दोनों इस पावर का कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते है। आइये जानते है कि इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण क्या होता है- Investigation को हिन्दी में अन्वेषण कहते है और अन्वेषण का तात्पर्य साक्ष्य को एकत्र करने के उद्देश्य से की गई एक ऐसी कार्यवाही से है जो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी संज्ञेय आपराध की घटना के घटित होने की सूचने थाने के भार साधक अधिकारी को दी गयी हो और ऐसी आपराधिक घटना के संदर्भ में थाने का भार साधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जाँच -पडताल व छान-बीन करके यह मालूम करना है कि क्या अपराध हुआ, कैसे अपराध हुआ और कौन-कौन व्यक्ति उस अपराध में शामिल थे इस प्रकार साक्ष्य को एकत्रित करने हेतु की गयी इस कार्यवाही को इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण कहा जाता है ।
क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण कर सकता है?
मजिस्ट्रेट स्वंम कभी अन्वेषण (investigation) नहीं कर सकता है । मजिस्ट्रेट केवल जाँच (inquiry) व विचारण(Trial) कर सकता है।यहाँ यह बताना महत्तवपूर्ण होगा कि अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य का एकत्रीकरण करना है।जब थाने के भार साधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त होती है तब ऐसा पुलिसअधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण कर सकता है। जबकि असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण नहीं कर सकता है। इन्वेस्टीगेशन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय-12 (पुलिस को सूचना और उसकी इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण की शक्तियों) जो धारा 154-176 के प्रावधानों में विस्तार से दिया गया है। इसअध्याय में इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण शब्द को धारा 2(ज) या Section 2 (h) में परिभाषित किया गया है
अन्वेषण की परिभाषा:-धारा 2(ज)
“अन्वेषण” के अन्तर्गत वे सब कार्यवाहियां है इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या (मजिस्ट्रेट से भिन्न) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित प्राधिक्रत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाय
Definition of Investigation: -Section 2 (h)
“Investigation” includes all the proceeding under this Code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person (other than a Magistrate) who is authorised by a Magistrate in this behalf.
इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण के क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं?
अन्वेषण की कार्यवाही में दो महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित होते हैं-
(i) संदेहयुक्त अपराधकर्ता (Drought full offender ) की तलाशी एवं उसकी गिरफ्तारी
(ii) साक्ष्य के एकत्रित करने के लिए आवश्यक स्थानों की तलाशी और आवश्यक वस्तुओं की जब्ती
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट आफ एम० पी० बनाम मुबारक-1959 के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि अन्वेषण के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं-
- घटना स्थल पर Investigating officer का पहुंचना।
- मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को उसके द्वारा सुनिश्चित किया जाना।
- अन्वेषण के लिए आवश्यक वस्तुओं की खोज तथा संदेहयुक्त अपराधकर्ता को गिरफ्तार करना।
- मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों की परीक्षा एवं उनके कथनों को अभिलिखित करना।
- यदि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पर्याप्त आधार हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र तैयार करना।
इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण में पुलिस अधिकारी से सम्बन्धित कुछ प्रावधान –
आपराधिक मामलों के इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण में पुलिस अधिकारी मुख्य अभिकरण की भूमिका निभाते हैं। इसी उद्देश्य की पूरा करने के लिए, पुलिस अधिकारियों को इन्वेस्टीगेशन के मामले में विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है। ये पुलिस अधिकारी आपराधिक मामलों के अन्वेषण में तथ्य तथा परिस्थितियों का पता लगाने के साथ-साथ मामले से परिचित व्यक्तियों की परीक्षा भी कर सकते हैं एवं उनके कथनों को अभिलिखित कर सकते हैं। ये पुलिस अधिकारी अन्वेषण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी स्थान की तलाशी ले सकते हैं एवं किसी ऐसी वस्तु की जब्ती कर सकता है जो अन्वेषण के लिए अपेक्षित हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अनुसार, पुलिस अधिकारी मामले से सम्बन्धित किसी साक्षी की परीक्षा कर सकते है एवं उसके अभिकथनों को लेखबद्ध कर सकता है तथा मामले से परिचित व्यक्तियों की अपने समक्ष उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता हैऔर धारा 160 का Notice दे सकता है।पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की शक्ति आपराधिक मामले की प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण आरम्भ कर सकता है जबकि असंज्ञेय मामले में कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही अन्वेषण कर सकता है।
इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण में न्यायपालिका से सम्बन्धित कुछ प्रावधान-
जहाँ तक इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण के विषय में पुलिस अधिकारी एवं न्यायपालिका का सम्बन्ध है इस संदर्भ में विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया है कि पुलिस द्वारा किये जा रहे इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण के हर प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए, किन्तु उसे अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ विधि आयोग ने यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट इसबात के लिए अधिकृत नहीं है कि वह अन्वेषण की रीति का निर्देशन करे। प्रिवी कौंसिल ने किंग इम्परर बनाम ख्वाजा नजीर अहमद 1945 के मामले में प्रिवी कौंसिल ने यह संप्रेक्षित किया कि न्यायपालिका एवं पुलिस के कृत्य एक दूसरे के सम्पूरक हैं और फिर भी पारस्परिक समायोजन को स्थापित करते हुए इन दोनों के द्वारा अपने कर्तव्यों का अनुपालन केवल विधि एवं आदेश के अनुपालन में किया जायेगा। बाद में एच० एन०रिशबुद बनाम स्टेट आफ देहली 1955 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मत की पुष्टि की है। ये Judgment आप के पढने के लिए Indiankanoon से लिया गया है।
यदि पुलिस अधिकारी पीडित को उपचार देने से इंकार कर देती है तो वह पीडित व्यक्ति क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। किसी अपराध से सम्बद्ध व्यक्ति से यह अपेक्षित नहीं है कि वह आवश्यक रूप से पुलिस अधिकारी के समक्ष उपचार के लिए जाये, वह बिना पुलिस अधिकारी के समक्ष गये ही सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर अपराध के संदर्भ में परिवाद प्रस्तुत कर सकता है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान किया जा सकता है अपराध के संज्ञान के पश्चात् मजिस्ट्रेट अपराध के संदर्भ में विचारण प्रारम्भ कर सकता है दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है, क्योंकि यदि पुलिस अधिकारी द्वारा व्यक्ति को समुचित उपचार नहीं प्रदत्त किया जाता है तो वह सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष जा सकता है।उपरोक्त स्थिति में अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को इस बात के लिए अधिकृत कर सकता है कि वह किसी अपराध के विषय में अन्वेषण का कार्य संपन्न करे, इस प्रकार अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पास अन्वेषण के संदर्भ में वे सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो एक पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अन्वेषण के संदर्भ में प्राप्त होती हैं किन्तु इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण करने के लिए अधिकृत कोई निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं रखता है।
संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को सूचना-धारा-154
धारा 154 सी.आर.पी.सी. को तीन उप-खण्डों विभाजित किया गया है। यह धारा किसी संज्ञेय अपराध के घटना के घटित होने की सूचना से सम्बन्धित है। कोई भी व्यक्ति ऐसी संज्ञेय अपराध की घटना के घटित होने की सूचना, पुलिस अधिकारी को दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में संज्ञेय अपराध के किये जाने की सूचना किस प्रकार पुलिस अधिकारी को दी जायेगी इसका वर्णन किया गया है।इस प्रकार यह धारा उस रीति का वर्णन करती है। जिस रीति से किसी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है और उसके द्वारा उसे लेखबद्ध किया जाता है यहाँ यह भी कहा जा सकता है ऐसी दी गई सूचना को ही F.I.R. प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। यह F.I.R. ही दंड विधि को गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से थाने के पुलिस अधिकारी को दी जाती है ताकि वह अपराध के संदर्भ में समुचित कार्यवाही को अग्रसर होकर इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण प्रारम्भ कर सके। धारा 154(1), धारा 154(2) तथा धारा 154(3) की महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार है-
- धारा 154(1) में संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित हो सकती है। यह थाना प्रभारी को सम्वोधित की जानी चाहिए।यदि सूचना मौखिक दी गयी है तो थाना प्रभारी इसे लेखबध्द करेगा या करवायेगा। इसे सूचना दाता को पढकर सुनायेगा। प्रत्येक F.I.R. पर सूचनादाता को हस्ताक्षर होने आवश्यक है।इस सूचना का साराशं सामान्य डायरी में इंकित किया जायेगा, F.I.R. किसी भी थाने में कराई जा सकती है केवल संज्ञेय इपराध में F.I.R. दर्ज कराई जा सकती है।
- धारा 154(2) F.I.R. की एक प्रति निशुल्क तथा तत्काल सूचनादाता को दी जाएगी।
- धारा 154(3) यदि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी F.I.R. को लिखने से इन्कार कर देता है तो पीडित व्यक्ति सूचना का लिखित सारांश डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक के पास भेज सकता है तो पुलिस अधीक्षक स्वमं या अपने किसी अधिनस्त पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेष्ण करा सकता है।
इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण पुलिस अधिकारी को प्रदत्त एक सांविधिक अधिकार (statutory right) है जिसमें न्यायपालिका द्वारा न तो हस्तक्षेप किया जा सकता है और न ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है।F.I.R. में जहां पर किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट नहीं होता है तो वहां पर पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण को बन्द कर देना चाहिए। नहीं तो उच्च न्यायालय इस स्थिति में अपनी अन्तर्निहित शक्ति धारा 482 या रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके अन्वेषण की कार्यवाही को समाप्त कर सकता है।इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण के प्रक्रम पर की गई कोईअनियमितता अन्वेषण की कार्यवाही को प्रभावहीन नहीं बना देती है अतः इन्वेस्टीगेशन के प्रक्रम पर हुई किसी अनियमितता मात्र से ही अन्वेषण की कार्यवाही प्रभावहीन नहीं मानी जाती है। लीलाराम बनाम हरयाणा राज्य (1999) 9 SCC 525) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि अन्वेषण की अवैधता अथवा अनियमितता अभियोजन पक्ष को निरस्त करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं निर्मित करती है।
असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को सूचना-धारा-155
- धारा-155 (1)के अनुसार,असंज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी उसका सारशं विहित पुस्तिका में इंगित करेगा और वह सूचनादाता को मजिस्ट्रेट को संदर्भित कर देगा।
- धारा-155 (2) के अनुसार, कोई पुलिस अधिकारी सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिनाअसंज्ञेय मामले में इन्वेस्टीगेशन नही करेगा।
- धारा-155 (3) के अनुसार,मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त होने पर पुलिस की समस्त शक्तियो प्राप्त जायेगी (बिना वारण्ट गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय)
- धारा-155 (4) के अनुसार,जब दो या दो से अधिक अपराधों से सम्वन्धित मामलों में से यदि कोई एक भी मामला संज्ञेय होने पर सम्पूर्ण मामले को संज्ञेय माना जायेगा।
इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण की क्या शक्ति तथा प्रकिया होती है?
- थाना प्रभारी संज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण कर सकता है धारा 190 के अन्तर्गत संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट इन्वेस्टीगेशन आदेशित कर सकता है।
- संज्ञेय अपराध या मामले का संदेह होने पर थाना प्रभारी सक्षम मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। यदि अन्वेषण न करने का निर्णय किया गया है तो रिपोर्ट में उसका भी उल्लेख होगा। रिपोर्ट के साथ I.R. की कोपी तथा अन्य सूचना भी भेजी जाएगी।
- साक्षियों की उपस्थित हेतु लिखित आदेश जारी करने की शक्ति।(धारा 160)
- पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर जाएगा या अधिनस्त अधिकारी को भेजेगा ( जिससे अपराध की तथ्य एवं परिस्थितिक का पता लगा सके और उस अपराध से सम्बधित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सके)
- प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितिक से परिचित व्यक्ति मौखिक परीक्षा करने की शक्ति।(धारा 161)
- तलाशी की शक्ति।(धारा 165)
- साक्ष्य अपर्याप्त होने पर आभियुक्त की अभिमुक्ति।(धारा 169)
- साक्ष्य पर्याप्त होने पर आभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजने या जमानत पर रिहा करने की शक्ति।(धारा 170)
- इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण हेतु केश डायरी तैयार करना(धारा 172)
- इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण पूर्ण हो जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना (धारा 173)
- यदि अभियुक्त नामित है तथा अपराध गम्भीर नहीं है या इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण करने के पर्याप्त आधार नहीं है तो पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर न जाने का निर्णय ले सकता है वह इन्वेस्टीगेशन न करने का भी निर्णय ले सकता है ऐसी स्थित में वह सूचनादाता को इन्वेस्टीगेशन न करने की सूचना देता है।
इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण के सम्बध में मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद की क्या प्रकिया है-
यदि थाना प्रभारी F.I.R. को नहीं लिखता हैऔर पीडित व्यक्ति द्वारा सूचना का लिखित सारांश डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी भेज दिया जाता है इस के बाबजूद भी यदि अन्वेष्ण प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो वह पीडित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) में परिवाद दाखिल कर सकता हैऔर ऐसे परिवाद पर मजिस्ट्रेट धारा 190 के अन्तर्गत संज्ञान लेता सकता है और वह पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के लिए आदेशित करता है। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि धारा 190(1)(a) के उपबंधों के अनुसार मजिस्ट्रेट इस बात के लिए आबद्ध नहीं है कि वह परिवाद प्राप्त होने पर आवश्यक रूप से अपराध का संज्ञान कर ले, यह उसके विवेक पर आधारित है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध का घटित होने का किसी परिवाद से प्रकट होता है तो वह मजिस्ट्रेट उस मामले में अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकता है। वहाँ ऐसा मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अपराध का संज्ञान करेगा।
धारा 202 (1) के अनुसार,यदि मजिस्ट्रेट परिवाद पर अपराध का संज्ञान कर लेता है और उसे अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी के पास नहीं भेज देता है तो वह अभियुक्त के विरूद्ध समन या वारंट जारी कर सकता है या स्वयं मामले में कोई जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अन्वेषण का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट यह पता लगाने के लिए करता है जिससे यह पता चल सके कि किसी कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार है या नहीं। तत्पश्चात् अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाती है।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ पर धारा 202 के अधीन कोई परिवाद अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् पुलिस अधिकारी के पास अन्वेषण के लिए भेजा जाता है तो उस स्थिति में पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के संदर्भ में वे सभी शक्तियां प्राप्त रहती हैं जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के संदर्भ में उसे प्राप्त होती हैं अन्वेषण के पश्चात् प्राप्त पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट इस उद्देश्य सह उपयोगी होती है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार है अथवा नहीं पुलिस रिपोर्ट इसलिए भी उपयोगी होती है कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई आदेशिका जारी की जाय अथवा परिवाद को खारिज कर दिया जाय।
इस प्रकार उक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट होता है कि किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित दशाओं में प्रारम्भ की जाती है.
(i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन किसी संज्ञेय अपराध के संदर्भ में F.I.R. दर्ज कराने पर इस स्थिति में अन्वेषण की कार्यवाही धारा 157 (1) तथा 156 (1) के अधीन प्रारम्भ की जाती है।
(ii) जहाँ पर किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) के अधीन किसी असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया है,
(iii) जहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध के संदर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया है और मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पूर्व परिवाद को अन्वेषण हेतु धारा 156(3) के अधीन पुलिस अधिकारी को प्रेषित कर देता है.
(iv) जहाँ पर अपने समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान कर लेता है और तत्पश्चात् परिवाद को पुलिस अधिकारी के पास अन्वेषण हेतु प्रेषित करता है। इस स्थिति में मजिस्ट्रेट परिवाद को धारा 202 (1) तथा 203 के अधीन पुलिस अधिकारी के पास इस बात के अन्वेषण के लिए भेजता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है अथवा नहीं।
धारा 156 (3) तथा धारा 202 में यह सम्बन्ध है कि एक मजिस्ट्रेट इस बात के लिए अधिकृत है वह दंड प्रक्रिया संहिता की दोनों धाराओं (धारा 156 (3) तथा धारा 200 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है.
मधुबाला बनाम सुरेश कुमार (1997) 8 SCC 476) के मामले में कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष का परिवाद किया जाता है और वह मामला संज्ञेय अपराध होता है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को उस मामले का पंजीकरण करने एवं उसका अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है:
धारा 156 (3)और धारा 202 (1) क्या अंतर है:
(a) धारा 156 (3) के अधीन अन्वेषण करने के लिए आदेश किसी अपराध का संज्ञान करने के पूर्व दिया जाता है जबकि धारा 202 (1) के अधीन अन्वेषण काआदेश किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् किया जाता है
(b) जहाँ पर मजिस्ट्रेट परिवादी की परीक्षा किये बिना ही अन्वेषण के लिए आदेश किसी पुलिस अधिकारी को देता है तो वहाँ पर यह समझा जायेगा कि उसने अपराध का संज्ञान नहीं लिया है और इस प्रकार अन्वेषण के लिए दिया गया आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन माना जायेगा।
जब कोई मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) या धारा 156 (3) के अधीन अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी को प्रेषित किया जाता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण करने के पश्चात् धारा 173 में वर्णित पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।यदि मजिस्ट्रेट इस प्रकार प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट से सहमत है कि कार्यवाही करने के लिए आधार है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(b) केअधीन पुलिस रिपोर्ट पर मामले का संज्ञान कार सकता है, किन्तु यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो वह पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान न करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) (a) के अधीन प्रस्तुत की गई आरम्भिक परिवाद पर मामले का संज्ञान करेगा तथा परिवादी की परीक्षा करने के लिए आदेशिका जारी करेगा। इसके अतिरिक्त यदि पुलिस रिपोर्ट में उल्लिखित इस कथन से मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह कार्यवाही को समाप्त कर देगा।
निर्ष्कष:-
साथियों आज हमने इस लेख के मध्यम से “इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण क्या होता है और इसकी क्या प्रकिया होती है” के बारे में सरल भाषा में अध्यन करके समझने प्रयास किया है यह साक्ष्य को एकत्र करने के उद्देश्य से की गई एक कार्यवाही है जिसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है। मुझे आशा है किइस लेख से आपको अवश्य ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी जो निश्चित ही आप के काम आयेगी। यहाँ तक पढने के लिए धन्नयवाद।
FAQ:
Q:Investigation meaning in Hindi?
Ans: Investigation को हिन्दी में “अन्वेषण “ या “जाँच -पडताल” कहते हैऔर Investigation का उद्देश्य साक्ष्य को एकत्रीकरण करना है।
Q:इन्वेस्टीगेशन का मतलब क्या होता है?
Ans: “Investigation” को हिन्दी में अन्वेषण कहते है और Investigation का तात्पर्य साक्ष्य को एकत्र करने के उद्देश्य से की गई एक ऐसी कार्यवाही से है जो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छान-बीन करके यह मालूम करना है कि क्या अपराध हुआ, कैसे अपराध हुआऔर कौन-कौन व्यक्ति उस अपराध में शामिल थे इसी साक्ष्य एकत्रित करने लिए की गयी कार्यवाही को इन्वेस्टीगेशन यानी अन्वेषण कहा जाता है ।
Q:Investigation kon karta hai?
Ans:” Investigation” थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी संज्ञेय आपराध की घटना के घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर। ऐसे अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छान-बीन करके यह मालूम करना है कि क्या अपराध हुआ, कैसे अपराध हुआ और कौन-कौन व्यक्ति उस अपराध में शामिल था।
Q: Police Officer kab Investigation karne se Inkar kar Sakta hai in Hindi?
Ans:पुलिस अधिकारी Investigation करने से इंकार कर सकता है यदि Investigating Officer को असंज्ञेय आपराध की घटना के घटित होने की सूचना प्राप्त हो। धारा-155 CrPC के अनुसार , ऐसा पुलिस अधिकारी सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना असंज्ञेय मामले में इन्वेस्टीगेशन नहीं करेगा।
Q:धारा 156 (3)और धारा 202 (1) क्या अंतर है?
Ans:धारा 156 (3) के अधीन अन्वेषण करने के लिए आदेश किसी अपराध का संज्ञान करने के पूर्व दिया जाता है जबकि धारा 202 (1) के अधीन अन्वेषण काआदेश किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् किया जाता है


